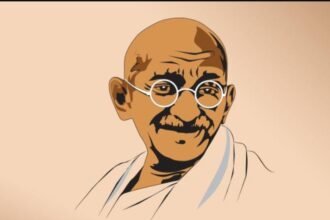लोकतंत्र में सिनेमा कभी केवल मनोरंजन का साधन नहीं रहा। जब से चलती तस्वीरों ने भीड़ को एक साथ हंसना, रोना और तालियां बजाना सिखाया, तभी से यह स्पष्ट हो गया था कि सिनेमा केवल कहानी नहीं सुनाता, वह सोच को भी दिशा देता है। यही वजह है कि बहुत जल्दी सता, सरकारों और वैचारिक समूहों ने सिनेमा की शक्ति को पहचाना। यहीं से प्रोपेगेंडा फिल्मों की यात्रा शुरू होती है, ऐसी फिल्में जिनका उद्देश्य सवाल खड़े करना नहीं, बल्कि दर्शक को एक तय निष्कर्ष तक भावनात्मक रूप से पहुंचाना होता है।
प्रोपेगेंडा फिल्मों की सबसे खास बात यह है कि वे अक्सर सीधे झूठ नहीं बोलतीं। वे अधूरे सच को पूरे सच की तरह पेश करती हैं। कुछ घटनाओं, कुछ चेहरों और कुछ भावनाओं को इतना उभार दिया जाता है कि बाकी सच्चाइयों अपने-आप अदृश्य हो जाती हैं। झंडा, संगीत, अनुशासन, नायकत्व और सामूहिक गर्व जैसे तत्व दर्शक के भावनात्मक मस्तिष्क को सक्रिय करते हैं, जहां तर्क और जटिलता के लिए बहुत कम जगह बचती है। परिणाम यह होता है कि भावनाएं धीरे-धीरे प्रमाण का स्थान लेने लगती है।
इस प्रवृत्ति की जड़ें बीसवीं सदी के शुरुआती दशकों में मिलती हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पहली बार सरकारों ने सिनेमा को संगठित ढंग से जनसमर्थन जुटाने के लिए इस्तेमाल किया। युद्ध को गौरवपूर्ण, बलिदान को पवित्र और दुश्मन को अमानवीय दिखाने वाली फ़िल्में और न्यूजरील्स बनाई गई। सिनेमा का यह दौर सूचना से अधिक भावना पर आधारित था। उस समय दर्शक के पास वैकल्पिक स्रोत सीमित थे. इसलिए जो परदे पर दिखा, वही सच बन गया। यहीं से यह समझ विकसित हुई कि सिनेमा भाषणों और अखबारों से कहीं अधिक प्रभावी है, क्योंकि वह सीधे आंखों और भावनाओं से संवाद करता है।
युद्ध के बाद यह प्रयोग और व्यवस्थित हुआ। कुछ देशों में सिनेमा को खुलकर वैचारिक औजार के रूप में अपनाया गया। सोवियत संघ में फिल्मों को विचारधारा की कक्षा माना गया। क्रांति, वर्ग-संघर्ष और समाजवादी आदर्शी को नैतिक सत्य की तरह प्रस्तुत किया गया। यहां प्रोपेगेंडा छुपा नहीं था, वह घोषित था। लंबे समय तक यह इसलिए काम करता रहा क्योंकि परदे पर दिखाई जा रही दुनिया और आम जनता के अनुभवों के बीच बहुत बड़ा अंतर नहीं था। लेकिन जैसे-जैसे रोज़मर्रा की सच्चाइयों परदे की चमक से टकराने लर्जी, वैचारिक थकान भी बढ़ने लगी।
इसी दौर में नाजी जर्मनी ने प्रोपेगेंडा सिनेमा को सबसे आक्रामक और खतरनाक रूप दिया। वहां फिल्में केवल समर्थन जुटाने का माध्यम नहीं थीं, बल्कि सता की वैचारिक रीढ़ थीं। सिनेमा के जरिये नेता को मिथक में बदला गया, भीड़ को अनुशासन और गर्व के प्रतीकों में ढाला गया और असहमति को राष्ट्रविरोध के रूप में पेश किया गया। तकनीकी दृष्टि से ये फिल्में अत्यंत प्रभावशाली थी, लेकिन नैतिक रूप से विनाशकारी।
प्रोपेगेंडा फिल्में इसलिए काम करती है क्योंकि वे अक्सर असुरक्षा और भय के दौर में सामने आती है। जब समाज किसी संकट, युद्ध या पहचान के संकट से गुजर रहा होता है, तब लोग जटिल सवालों के बजाय सरल जवाब चाहते हैं। ऐसी स्थिति में हम बनाम वे की कहानी, अचूक नायक और भावनात्मक एकजुटता आकर्षक लगने लगती है। सिनेमा इस मनोविज्ञान को बहुत अच्छे से समझता है और उसी के अनुसार अपनी भाषा गढ़ता है।
अमेरिका का रास्ता इन दोनों से थोड़ा अलग था। जहां प्रोपेगेंडा” शब्द से परहेज़ किया गया, लेकिन सिनेमा को राष्ट्रीय नैरेटिव गढ़ने के लिए सक्रिय रूप से इस्तेमाल किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फिल्मों ने लोकतंत्र और स्वतंत्रता को नैतिक अनिवार्यता के रूप में प्रस्तुत किया। शीत युद्ध में यही सिनेमा साम्यवाद-विरोध का वाहक बना। दर्शक को लगा कि वह केवल कहानी देख रहा है, जबकि कहानी उसे यह भी सिखा रही थी कि अच्छा और बुरा कौन है। इस सूक्ष्मता ने अमेरिकी प्रोपेगेंडा को वैश्विक प्रभाव दिया। लेकिन वियतनाम युद्ध के दौरान जब टेलीविजन ने युद्ध की कच्ची सच्चाइयों घर-घर पहुंचाई, तो फ़िल्मी नैरेटिव टूट गया।
नाजी जर्मनी, सोवियत संघ और अमेरिका तीनों के उदाहरण बताते है कि प्रोपेगेंडा तब सबसे शक्तिशाली होता है जब वह समाज की मनोवैज्ञानिक ज़रूरतों से मेल खाता है, और सबसे खतरनाक तब, जब वह आलोचना की जगह बंद कर देता है।
इसलिए इतिहास का यह अध्याय केवल अतीत की कहानी नहीं है। यह एक चेतावनी है- कि चाहे प्रोपेगेंडा कितना भी प्रभावी क्यों न लगे, यदि वह सवालों की जगह बंद करता है, तो अंततः वही शक्ति समाज को भीतर से खोखला कर देती है। अगले चरण में यही चेतावनी भारत के संदर्भ में और अधिक प्रासंगिक हो जाती है। जहां सिनेमा की पहुंच, भावनात्मक तीव्रता और सामाजिक विविधता- तीनों एक साथ मौजूद हैं।
भारत में सिनेमा कभी केवल मनोरंजन नहीं रहा। आज़ादी के साथ ही यह राष्ट्र की भावनात्मक भाषा बन गया-एक ऐसा माध्यम, जिसके जरिये न केवल कहानियां कही गई, बल्कि नए देश की पहचान भी गढ़ी गई। भाषा, धर्म, क्षेत्र और वर्ग के बीच साझा नागरिक चेतना बनाना आसान नहीं था। इसी दौर में सरकार ने सिनेमा की ताकत को पहचाना और Films Division of India के माध्यम से एक सुनियोजित प्रयास शुरू किया। हर सिनेमाघर में मुख्य फ़िल्म से पहले दिखाई जाने वाली लघु फिल्में विकास योजनाओं, लोकतंत्र, वैज्ञानिक सोच और राष्ट्रीय एकता का संदेश देती थीं। यह प्रोपेगेंडा आक्रामक नहीं था। यह धीरे बोलता था, लेकिन लगातार बोलता था। दर्शक इसे आदेश नहीं, सामान्य सूचना की तरह ग्रहण करता गया। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी।
इस शुरुआती दौर के प्रोपेगेंडा को अक्सर राष्ट्र-निर्माण का सिनेमा कहा जाता है। इसमें देशभक्ति थी, लेकिन शोर नहीं, संदेश था, ध्रुवीकरण भी नहीं था। यह वह समय था जब सिनेमा सरकार की नीतियों को वैध ठहराने से अधिक, नागरिकों को नए लोकतांत्रिक ढांचे से परिचित कराने का माध्यम बना। यहां प्रोपेगेंडा की भूमिका शिक्षात्मक थी, न कि वैचारिक वर्चस्व की।
1962 के भारत-चीन युद्ध ने इस संतुलन में पहला बड़ा भावनात्मक मोड लाया। युद्ध में मिली पराजय ने राष्ट्रीय आत्मविश्वास को गहरी चोट पहुंचाई। ऐसे समय में बनी हकीकत को भारतीय प्रोपेगेंडा सिनेमा का प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है। इस फिल्म का उद्देश्य स्पष्ट था-गिरे हुए मनोबल को उठाना। यहां प्रोपेगेंडा रक्षात्मक था। सैनिकों के बलिदान को सम्मान दिया गया, पीड़ा को स्वीकार किया गया और दुश्मन को कठोर दिखाया गया, लेकिन नायक को देवता नहीं बनाया गया। यह वह दौर था जब प्रोपेगेंडा का उद्देश्य समाज को स्थिर करना था न कि किसी वैचारिक निष्कर्ष को थोपना।
समय के साथ, विशेषकर 1990 के दशक में, भारतीय सिनेमा और राष्ट्रवाद का रिश्ता बदला। उदारीकरण के बाद बाजार की भूमिका बढी और सिनेमा भावनात्मक अनुभव के साथ-साथ उत्पाद भी बनने लगा। इसी दौर में Border जैसी फ़िल्मों ने युद्ध को एक भावनात्मक spectacle में बदल दिया। देशभक्ति, बलिदान, गीत और संवाद-सब कुछ इस तरह रचा गया कि दर्शक गर्व से भर जाए। राष्ट्रवाद अब बॉक्स ऑफिस की गारंटी बनने लगा।
2014 के बाद यह प्रवृत्ति और तीव्र हो गई। राष्ट्रवाद का स्वर हाई-वोल्टेज हुआ और सिनेमा में नायकवाद केंद्र में आ गया। Uri: The Surgical Strike जैसी फिल्मों ने सैन्य कार्रवाई को केवल रणनीतिक घटना नहीं, बल्कि भावनात्मक सत्य के रूप में प्रस्तुत किया। नायक अचूक दिखाई दिया, निर्णयों पर सवाल हाशिये पर चले गए और दर्शक से अपेक्षा की गई कि वह गर्व के साथ एक निश्चित निष्कर्ष स्वीकार करे। यहां प्रोपेगेंडा का उद्देश्य मनोबल बढ़ाने से आगे बढ़कर वैचारिक स्वीकृति तक पहुंचता दिखा।
इसी अवधि में कुछ फ़िल्मों ने ऐतिहासिक और सामाजिक त्रासदियों को एकमात्र नैरेटिव में बदल दिया। पीड़ा वास्तविक थी, लेकिन उसका प्रस्तुतिकरण ऐसा था कि जटिलताओं और बहुविध सच्चाइयों के लिए बहुत कम जगह बची। भावना इतनी प्रबल थी कि संवाद का स्थान संकुचित हो गया। यह वह बिंदु या जहां देशभक्ति और प्रोपेगेंडा के बीच की पतली रेखा और भी धुंधली हो गई।
ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के आगमन ने इस पूरे परिदृश्य को एक नया आयाम दिया। अब प्रोपेगेंडा केवल सिनेमाघर तक सीमित नहीं रहा। वेब सीरीज और फ़िल्में वास्तविक घटनाओं से प्रेरित कहानियों के रूप में सामने आने लगीं। एल्गोरिदम दर्शक की पसंद को पहचानकर उसी सोच को पृष्ट करने वाली सामग्री बार-बार परोसने लगे। दर्शक को यह भ्रम हुआ कि वह स्वतंत्र चुनाव कर रहा है, जबकि कंटेंट पहले से उसकी भावनात्मक और वैचारिक प्रवृत्तियों के अनुसार चुना जा चुका था। यहाँ प्रोपेगेंडा का प्रभाव तेज नहीं, बल्कि निरंतर और गहरा हो गया।
यह कहना ज़रूरी है कि यह इतिहास केवल आलोचना के लिए नहीं है। संकट के समय सिनेमा ने समाज को संभाला भी है। लेकिन इतिहास यह भी बताता है कि जब प्रोपेगेंडा स्थायी हो जाए और उसकी संख्या व प्रभाव मानवीय, प्रश्नात्मक और विविध सिनेमा से अधिक हो जाए, तो वह लोकतंत्र के लिए चुनौती बन जाता है। भारत का अनुभव इसी चौराहे पर खड़ा दिखाई देता है।
आज का संकट किसी एक फिल्म, किसी एक निर्देशक या किसी एक विचारधारा का नहीं है। संकट उस क्षण का है, जब किसी समाज में प्रोपेगेंडा-प्रधान फिल्मों की संख्या और प्रभाव सामान्य, मानवीय और प्रश्नात्मक सिनेमा से अधिक हो जाए। इतिहास बताता है कि यह स्थिति अचानक नहीं आती। यह धीरे-धीरे बनती है- इतनी धीरे कि समाज को इसका एहसास तब होता है, जब सोच की विविधता पहले ही संकुचित हो चुकी होती है।
सिनेमा का सबसे बड़ा प्रभाव उसकी आवृत्ति में होता है। एक बार देखी गई फिल्म प्रभाव डाल सकती है, लेकिन बार-बार देखी जाने वाली एक जैसी कहानियां सोच को आदत में बदल देती हैं। यहीं से नागरिक और अनुयायी के बीच की रेखा धुंधली होने लगती है।
आज के दौर का एक और बड़ा खतरा यह है कि भावनाओं को प्रमाण का विकल्प बना दिया गया है। झंडा, संगीत, आंसू और गर्व-ये सब महत्वपूर्ण मानवीय अनुभव हैं, लेकिन जब इन्हें नीति, इतिहास और निर्णयों की समीक्षा का स्थान दे दिया जाता है, तब लोकतांत्रिक संवाद ठहरने लगता है। इतिहास बताता है कि भावना से बनी सहमति तेज होती है, लेकिन टिकाऊ नहीं। जैसे ही वास्तविक जीवन की समस्याएं रोजगार, महंगाई, असमानता-भावनात्मक कथाओं से टकराती हैं, समाज में असंतोष पनपने लगता है।
यहीं पर नागरिक की भूमिका निर्णायक हो जाती है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच सेंसरशिप नहीं, बल्कि जागरूक नागरिक होता है। ऐसा नागरिक जो यह पूछने का साहस रखता है कि कहानी कौन सुना सुना रहा है। क्यों सुना रहा है और किसकी आवाज़ गायब है। इतिहास हमें यह नहीं सिखाता कि सिनेमा से डरना चाहिए; वह यह सिखाता है कि सिनेमा को समझना चाहिए। जब दर्शक यह पहचानने लगता है कि भावना कब सूचना का स्थान ले रही है, तभी प्रोपेगेंडा की सीमा तय होती है।
समाज के लिए चेतावनी भी यहीं छुपी है। यदि किसी देश में नीतियों, निर्णयों और इतिहास को सही ठहराने के लिए बार-बार फिल्मों का सहारा लिया जाने लगे, तो यह शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि वैधता का संकट होता है। लोकतंत्र में निर्णय तर्क, संवाद और जवाबदेही से टिकते हैं-भावनात्मक कथाओं से नहीं। जब सिनेमा नीति का बचाव करने लगे, तो समझना चाहिए कि संवाद कमजोर पड़ रहा है।
यह भी उतना ही सच है कि समाधान प्रतिबंध या सेंसरशिप नहीं है। इतिहास गवाह है कि विचारों को दबाने से वे और मजबूत होते हैं। समाधान संतुलन में है-ऐसे सिनेमा में जो राष्ट्रवाद के साथ-साथ मानवीय संवेदना, सामाजिक यथार्थ, व्यंग्य और असहमति को भी जगह दे। और ऐसे दर्शक में, जो तालियां बजाने के साथ-साथ सवाल पूछने की आदत भी बनाए रखे।

कुलदीप वशिष्ठ, स्वतंत्र पत्रकार
नोट – ये लेखक के निजी विचार हैं।