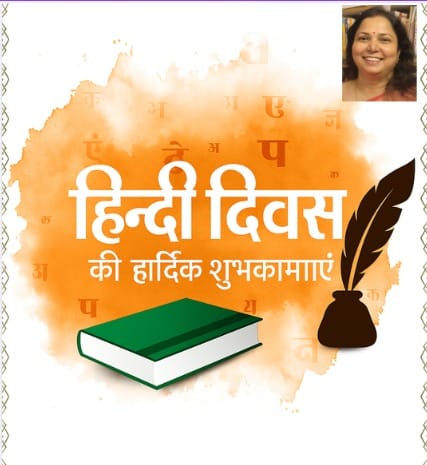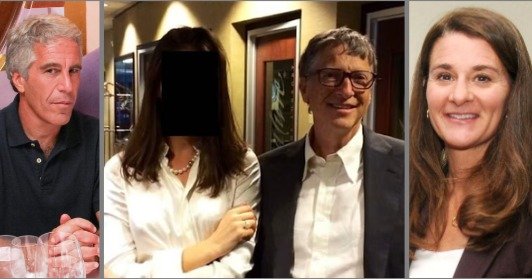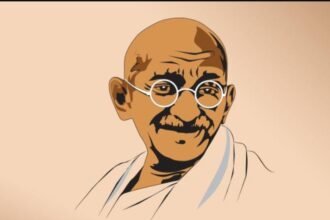हिंदी हमारी समृद्ध सांस्कृतिक, साहित्यिक और ऐतिहासिक विरासत की पहचान है. 14 सितंबर 1949 को हिंदी हमारे देश की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई. भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में हिंदी भाषा की सहज बोधगम्यता और स्वीकार्यता को देखते हुए स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों ने अपनी आंखों में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के सपने सजाए थे. हिंदी को इस स्थिति तक पहुंचने में गुजराती भाषी गांधी, मराठी भाषी बाल गंगाधर तिलक,बांग्ला भाषी केशवचंद्र सेन, दक्षिण के सी. राजगोपालाचारी, मोटुरी सत्यनारायण रेड्डी जैसे अनेकानेक हिंदी साधकों की बड़ी भूमिका रही है.
संविधान के आठवीं अनुसूची में प्रारंभ में कुल 15 भाषाएं थीं. आज और प्रांतीय और क्षेत्रीय भाषाओं को जोड़ते हुए उनकी कुल संख्या 22 तक पहुंच चुकी है. हिंदी के लिए विशिष्ट उपलब्धि यह है कि इन सभी भारतीय भाषाओं में हिंदी को मुखिया का दायित्व मिला है. नायक के रूप में हिंदी भाषा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण और उपादेय हो जाती है क्योंकि हिंदी मूलतः एक भाषिक समूह है. भाषिक समूह से तात्पर्य भाषा का वह रूप जो भिन्न-भिन्न भाषाओं के शब्दों को समावेशित करके बनता है. इस प्रकार हिंदी भाषा समावेशी प्रकृति की भाषा है. इसमें कुछ शब्द तत्सम , तो कुछ तद्भव ,कुछ देशज शब्द, कुछ विदेशी और कुछ संकर शब्दों का समावेश है. इस दृष्टि से भी हिंदी भाषा का नायकत्व और प्रासंगिक हो जाता है. वह अपने तमाम क्षेत्रीय और प्रांतीय भाषा के शब्दों को आत्मसात करते हुए ,उनसे सीधा संवाद स्थापित करते हुए, उनके शब्दों को अपने चलन में लाते हुए अपना स्वरूप निर्मित करती है. मराठी , बांग्ला जैसी भाषाएं हों अथवा अवधी, भोजपुरी, ब्रज जैसी बोलियां ,इन के शब्दों को हिंदी सहजता से आत्मसात करती है. समस्त भारतीय भाषाओं के समृद्ध साहित्यिक और ऐतिहासिक विरासत से वह अपना दाय ग्रहण कर अपने राष्ट्रीय स्वरूप का निर्माण करती है.
वैश्विक पटल पर हिंदी भाषा की स्थिति विकिपीडिया पर कभी तीसरी, कभी पांचवी विश्व भाषा के रूप में नजर आती है. यह स्थिति तब है जब हिंदी की अनेक उप भाषाओं ,आंतरिक बोलियों आदि को अलग रखा गया है. जनसंख्या की दृष्टि से हम विश्व की सबसे बड़ी ताकत है. उस दृष्टि से भी हिंदी बोलने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है. परंतु हिंदी के वैश्विक स्वरूप के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भारत से बाहर गए गिरमिटिया मजदूरों की है. मॉरीशस, त्रिनिदाद, टोबैगो ,सूरीनाम , नेटाल और फिजी जैसे अनेक देशों में गिरमिटिया मजदूरों ने अपने देश की संस्कृति के प्रतीक गंगाजल ,तुलसीदास , रामचरितमानस और अपनी बोली-बानी को अपने हृदय में संजो कर रखा. दु:सह कष्ट भोगते हुए भी उन्होंने अपनी बोली- बानी और संस्कृति को सुरक्षित रखा. आज उन सभी देशों में ये प्रवासी भारतीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जैसे अनेक उच्च पदों पर प्रतिष्ठित हैं. उनके त्याग और भारत के प्रति अपरिमित लगाव के कारण भारत देश की भाषा-बोली पूरे विश्व में व्याप्त हो पाई.
औद्योगिक क्रांति और सूचना क्रांति के इस युग में हिंदी ने इस नई कसौटी पर भी अपने आप को खरा उतारने का पूरा प्रयास किया है. अब वह कंप्यूटर की भाषा के रूप में भी दक्षता से कार्य कर रही है, स्वयं को तकनीकी रूप से सामर्थ्यवान बना रही है. हिंदी की इस विराट विकास यात्रा के साथ यह भी सत्य है हिंदी के व्यावहारिक क्रियान्वयन में कुछ समस्याएं और कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे भाषाई अंतर्विरोध, शैक्षणिक माध्यम के हेतु विषयानुरूप पारिभाषिक शब्दावली, हिंदी भाषा के अंतर्गत अनुसंधान- आविष्कार एवं अन्य वैश्विक भाषाओं की तुलना में तकनीकी दक्षता के क्षेत्र में बहुत कार्य करने की आवश्यकता है.
इसमें संदेह नहीं कि हिंदी भारत के मान सम्मान और पहचान की भाषा है,प्रत्येक भारतीय का गौरव है. कुल मिलाकर हिंदी की विकास यात्रा बहुत सुखद, आकर्षक और रोचक है तथा अशेष संभावनाओं से भरी हुई है. गांव, शहर, राज्य, राष्ट्र को जोडती हुई हिंदी आज वैश्विक पटल पर अपनी सार्थक उपस्थिति दर्ज करा रही है. इसके स्नेहिल संरक्षण , समावेशी प्रवृत्ति, ऐतिहासिक और भावात्मक कोश को देखकर ही कहा गया है-
मैं राष्ट्रगगन के मस्तक पर, सदियों से अंकित बिंदी हूँ,
मैं सब की जानी पहचानी, भारत की भाषा हिंदी हूँ.
लेखक
प्रो. हेमांशु सेन
हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश.