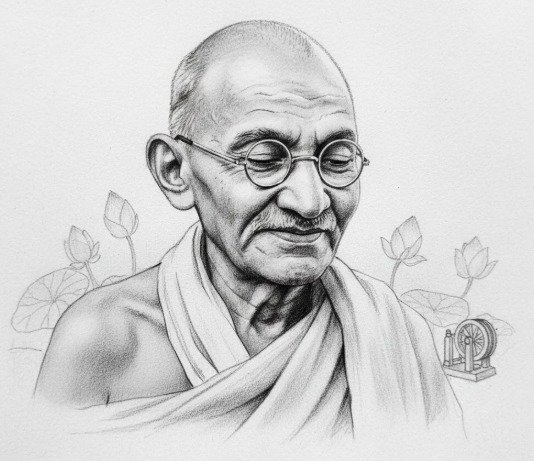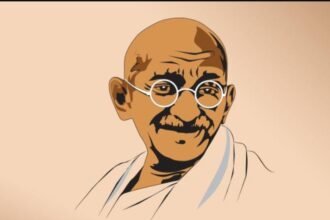गांधी — इतिहास नहीं, एक नैतिक परियोजना
इतिहास सामान्यतः घटनाओं का क्रम होता है—कब क्या हुआ, किसके कारण हुआ और सत्ता किसके हाथ में गई। लेकिन इतिहास अक्सर यह नहीं बताता कि उन घटनाओं में मनुष्य की नैतिक चेतना की क्या भूमिका थी। यहीं आकर महात्मा गांधी इतिहास से अलग दिखाई देते हैं। गांधी को केवल ऐतिहासिक व्यक्तित्व के रूप में देखना उनके साथ अन्याय होगा, क्योंकि वे स्वयं को कभी इतिहास की अंतिम व्याख्या नहीं मानते थे। वे एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक प्रश्न थे—और उससे भी आगे, एक ऐसी नैतिक परियोजना, जो आज भी अधूरी है।
गांधी को आमतौर पर भारत की आज़ादी के नायक के रूप में पढ़ा जाता है। यह पढ़ना गलत नहीं है, पर अधूरा अवश्य है। यदि गांधी केवल स्वतंत्रता संग्राम के नेता होते, तो 1947 के बाद उनका महत्व स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज़ादी के बाद भी गांधी पर बहस जारी रही—कभी उन्हें आदर्श बनाया गया, कभी अप्रासंगिक कहा गया, और कभी केवल औपचारिक श्रद्धांजलि तक सीमित कर दिया गया। यह निरंतर बहस इस बात का प्रमाण है कि गांधी किसी एक ऐतिहासिक क्षण में समाप्त नहीं होते। वे इतिहास का अध्याय नहीं, बल्कि नैतिक विवेक की एक सतत प्रक्रिया हैं।

गांधी स्वयं इतिहास को लेकर सजग थे। वे जानते थे कि सत्ता इतिहास को अपने अनुसार गढ़ती है। शायद यही कारण था कि उन्होंने अपने जीवन को ‘उपलब्धि’ नहीं, बल्कि ‘प्रयोग’ कहा। उनकी आत्मकथा “सत्य के प्रयोग” इस बात की घोषणा है कि वे स्वयं को अंतिम सत्य का स्वामी नहीं मानते थे, बल्कि सत्य की खोज में लगे एक साधक थे। राजनीति के क्षेत्र में यह स्वीकारोक्ति असाधारण थी, जहाँ नेता स्वयं को अचूक और अपरिहार्य मानने के आदी होते हैं।
गांधी की नैतिक परियोजना का अर्थ यह है कि उनका जीवन किसी तयशुदा खाके पर नहीं चला। उन्होंने बार-बार अपने निर्णयों पर पुनर्विचार किया, अपनी भूलों को स्वीकार किया और सार्वजनिक रूप से अपने रास्ते बदले। चौरी-चौरा के बाद असहयोग आंदोलन को वापस लेना इसका स्पष्ट उदाहरण है। राजनीतिक दृष्टि से यह निर्णय विवादास्पद हो सकता है, लेकिन नैतिक दृष्टि से यह गांधी के पूरे दर्शन को उजागर करता है। उनके लिए लक्ष्य से अधिक महत्वपूर्ण वह रास्ता था, जिस पर चलकर लक्ष्य तक पहुँचा जाए।
आधुनिक राजनीति अक्सर इस धारणा पर टिकी होती है कि उद्देश्य साधनों को उचित ठहरा देता है। गांधी ने इस सोच को जड़ से चुनौती दी। उनका मानना था कि यदि साधन ही दूषित हैं, तो उद्देश्य चाहे जितना पवित्र क्यों न हो, अंततः वह हिंसा और अन्याय को जन्म देगा। उनके लिए राजनीति और नैतिकता अलग-अलग क्षेत्र नहीं थे। राजनीति मानव जीवन का विस्तार थी, इसलिए उसमें वही मूल्य लागू होने चाहिए जो व्यक्तिगत जीवन में अपेक्षित हैं।
यही दृष्टि उन्हें अपने समय के अधिकांश नेताओं से अलग करती है। उनके लिए आज़ादी केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं थी, बल्कि भय, लोभ और घृणा से मुक्ति भी थी। यदि मनुष्य भीतर से गुलाम बना रहे, तो बाहरी स्वतंत्रता भी खोखली हो जाती है—यह गांधी के चिंतन का मूल था।
दक्षिण अफ़्रीका: अपमान, प्रतिरोध और सत्याग्रह का जन्म
1893 में जब गांधी दक्षिण अफ़्रीका पहुँचे, तब वे कोई आंदोलनकारी नहीं थे। वे एक युवा वकील थे, जिन्हें ब्रिटिश साम्राज्य की न्यायप्रियता पर भरोसा था। दक्षिण अफ़्रीका जाना उनके लिए एक पेशेवर अवसर भर था। लेकिन यही यात्रा उनके जीवन की दिशा बदलने वाली सिद्ध हुई।

दक्षिण अफ़्रीका उस समय नस्लीय भेदभाव की प्रयोगशाला था। कानून के माध्यम से श्वेत अल्पसंख्यक सत्ता एशियाई और अफ्रीकी समुदायों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना रही थी। पिटर्मैरिट्ज़बर्ग स्टेशन पर प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बावजूद गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाना केवल व्यक्तिगत अपमान नहीं था; वह उस भ्रम का अंत था कि साम्राज्य के भीतर न्याय सभी के लिए समान है।
उस रात गांधी के सामने दो रास्ते थे—अपमान स्वीकार कर लौट जाना, या अन्याय के विरुद्ध टिके रहना। उन्होंने दूसरा मार्ग चुना। यही निर्णय उन्हें एक पेशेवर वकील से नैतिक प्रतिरोध के मार्ग पर ले गया। शुरुआत में उन्होंने याचिकाएँ लिखीं और संवाद का रास्ता अपनाया, लेकिन धीरे-धीरे यह स्पष्ट हुआ कि जब कानून स्वयं अन्याय को वैध बना दे, तब केवल कानूनी लड़ाई पर्याप्त नहीं होती।
1906 में अनिवार्य पंजीकरण कानून के विरोध में गांधी ने ‘सत्याग्रह’ की अवधारणा प्रस्तुत की। यह केवल राजनीतिक रणनीति नहीं थी, बल्कि राजनीति की आत्मा का पुनर्निर्माण था। सत्याग्रह का अर्थ था—सत्य के लिए आग्रह, अन्यायपूर्ण कानून का उल्लंघन और दंड को स्वेच्छा से स्वीकार करना। इसमें हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं था, लेकिन कायरता के लिए भी नहीं।
दक्षिण अफ़्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग अत्यंत कठिन था। सत्याग्रहियों को जेलों में डाला गया, अत्याचार हुए, आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। स्वयं गांधी को भी कई बार कारावास झेलना पड़ा। लेकिन इन कष्टों ने आंदोलन को कमजोर नहीं किया, बल्कि उसकी नैतिक वैधता को और मज़बूत किया। पहली बार दुनिया ने देखा कि बिना हथियार उठाए भी सत्ता की नींव को हिलाया जा सकता है।
सत्याग्रह का दार्शनिक आधार
सत्याग्रह किसी एक परंपरा की उपज नहीं था। यह भगवद्गीता के कर्मयोग, जैन अहिंसा और टॉल्स्टॉय की नैतिक ईसाई दृष्टि का संगम था। गीता से गांधी ने यह सीखा कि मनुष्य कर्म का अधिकारी है, फल का नहीं। जैन परंपरा से उन्होंने अहिंसा को विचार, वाणी और कर्म—तीनों स्तरों पर अपनाने का आग्रह लिया। टॉल्स्टॉय से उन्होंने यह समझा कि बुराई का प्रतिकार हिंसा से नहीं, नैतिक दृढ़ता से किया जा सकता है।
गांधी के लिए अहिंसा कायरता नहीं थी। यह सक्रिय नैतिक साहस था—अन्याय को पहचानने और उसके सामने टिके रहने की क्षमता। सत्याग्रह में पीड़ा का स्वैच्छिक स्वीकार केंद्रीय तत्व था। गांधी मानते थे कि जब पीड़ित स्वयं कष्ट सहता है, तब वह अत्याचारी की नैतिक वैधता को चुनौती देता है। यह प्रतिशोध नहीं, आत्मबल की अभिव्यक्ति थी।
भारत आगमन: देश को समझने की चेतन यात्रा
1915 में भारत लौटने पर गांधी ने नेतृत्व की घोषणा नहीं की। उन्होंने पहले देश को समझने का निर्णय लिया। वे तीसरी श्रेणी में यात्रा करते हुए गाँव-गाँव घूमे। यह यात्रा प्रतीकात्मक नहीं थी; यह भारत की सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं को जानने का प्रयास था।
गांधी ने समझा कि भारत की समस्या केवल औपनिवेशिक शासन नहीं, बल्कि उसकी आंतरिक विषमताएँ भी हैं—किसान शोषण, जाति-व्यवस्था, अशिक्षा और स्त्रियों की स्थिति। चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के आंदोलनों में गांधी ने सत्याग्रह को भारतीय संदर्भ में ढाला। वे आंदोलन को जनता पर थोपते नहीं थे, बल्कि जनता की नैतिक तैयारी के अनुरूप गढ़ते थे।

उनके लिए स्वतंत्रता केवल सत्ता परिवर्तन नहीं थी, बल्कि समाज का नैतिक पुनर्निर्माण था। यही कारण है कि वे जाति, छुआछूत और सामाजिक असमानता को राजनीतिक संघर्ष से अलग नहीं मानते थे। गांधी राष्ट्र को केवल राजनीतिक इकाई नहीं, बल्कि नैतिक समुदाय मानते थे।
गांधी आज क्यों ज़रूरी हैं
गांधी किसी एक विचारधारा में पूरी तरह फिट नहीं बैठते। यही कारण है कि हर युग उन्हें अपने अनुसार ढालने की कोशिश करता है। लेकिन गांधी प्रतीक बनकर नहीं समझे जा सकते। वे एक जीवित नैतिक चुनौती हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि राजनीति केवल सत्ता-प्रबंधन नहीं, बल्कि नैतिक जिम्मेदारी है।
इसी अर्थ में गांधी हर सत्ता के लिए असुविधाजनक हैं। वे किसी एक विचारधारा में पूरी तरह फिट नहीं बैठते। यही कारण है कि हर युग उन्हें अपने अनुसार ढालने की कोशिश करता है। लेकिन गांधी प्रतीक बनकर नहीं समझे जा सकते। वे एक जीवित नैतिक चुनौती हैं।
अगले भाग में हम देखेंगे कि गांधी की यह नैतिक परियोजना भारत की ज़मीन पर कैसे उतरती है—चंपारण से दांडी तक के आंदोलनों में अनुशासन कैसे राजनीति की आत्मा बनता है, कैसे आंदोलन लक्ष्य नहीं बल्कि साधन बनते हैं, धर्म निजी आस्था से आगे बढ़कर नैतिक सेतु का रूप लेता है, और क्यों गांधी हर बदलाव की शुरुआत सत्ता से नहीं, व्यक्ति से करने का आग्रह करते हैं।
(क्रमशः — भाग 2 अगले दिन)

(नोट : ये लेखक के निजी विचार हैं।)